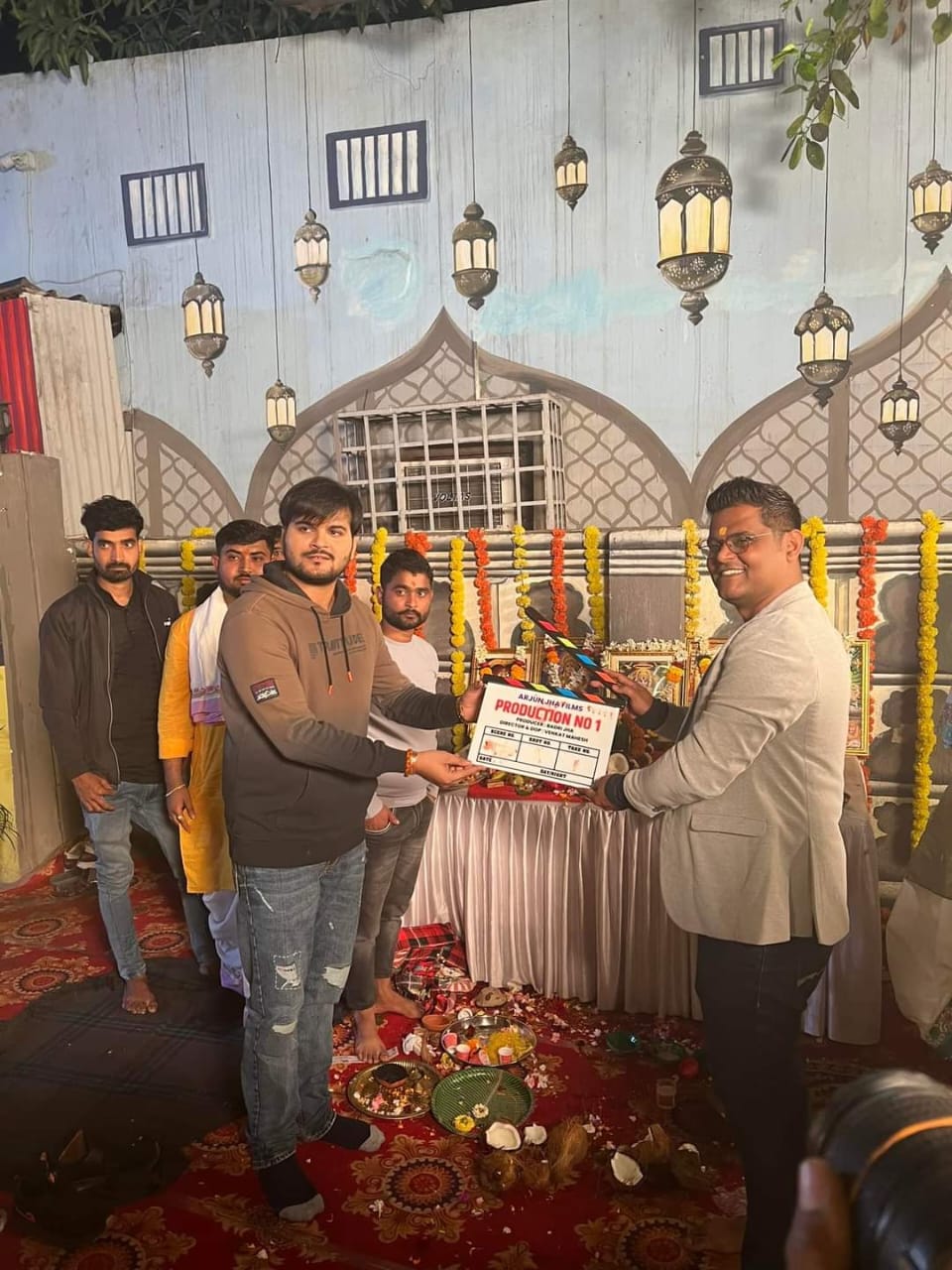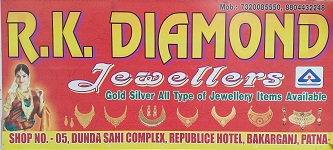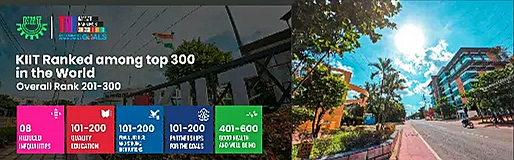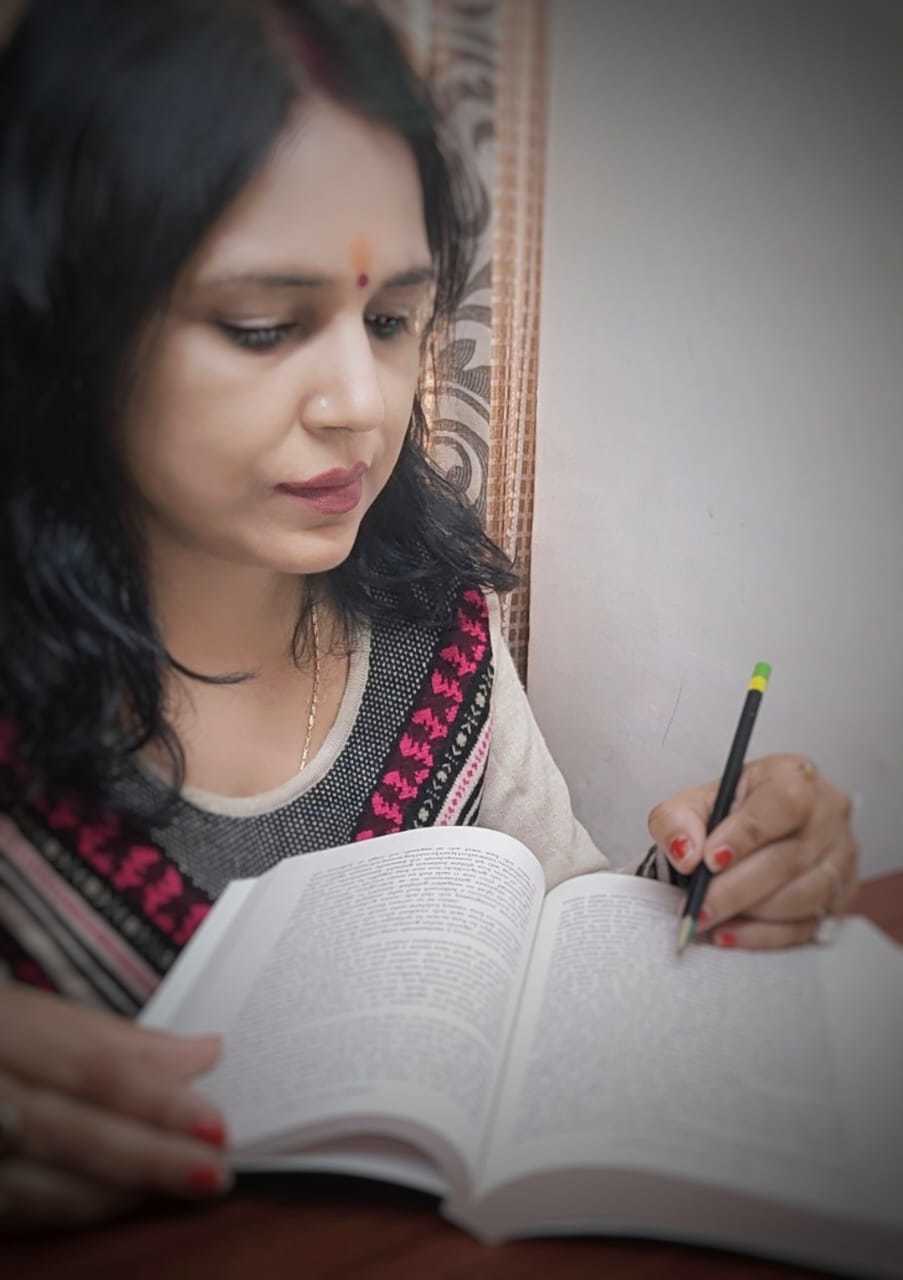हम बगावत क्यों नहीं करते?
भारत में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। दुनिया के एक-तिहाई निर्धनतम लोग यहां रहते हैं। उचित उपचार व पालन-पोषण के अभाव में हर साल पांच वर्ष से कम आयु के सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। 60 फीसदी से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे दैनिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। हमारे यहां टॉयलेट नहीं हैं और न मकान हैं। दुनिया के सर्वाधिक बेघर हमारे यहां हैं। झुग्गी में रहने वालों की संख्या ब्रिटेन की आबादी के तीन गुने से ज्यादा है। डॉलर वाले अरबपतियों की संख्यामें हम दुनिया में छठे स्थान पर हैं। शीर्ष 100 भारतीय अरबपतियों के पास 175 अरब डॉलर की सामूहिक संपत्ति है। हॉन्गकांग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस से ज्यादा। मुंबई (अपनी झुग्गी बस्तियों के बावजूद) दुनिया के 20 अरबपति शहरों में शामिल है। यह अपने यहां दुनिया का सबसे महंगा घर होने की शेखी भी बघारता है। यह स्वर्ण नगरी है। दुनिया के किसी अन्य शहर की बजाय कहीं ज्यादा जिंदगियां व कॅरिअर यहां बने और बिगड़े हैं। ऐसी अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक समृद्धि के बावजूद भारत एक चुनाव से दूसरे चुनाव की ओर जीवंत, धड़कते, फलते-फूलते लोकतंत्र के रूप में हिचकोले खाता रहता है। बेशक, समुदायों व जातियों के बीच कभी-कभार हिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इनसे निपट लिया जाता है और लोग जल्दी ही उसी सामुदायिक जिंदगी में लौट आते हैं, जिसे अर्थशास्त्री व राजनयिक जॉन गालब्रेथ ने कार्यशील अराजकता कहा था। भ्रष्ट राजनेताओं से व्यापक मोहभंग के बावजूद हमारे चुनावों में मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहता है। देश पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाली हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को हाल ही में उस पार्टी ने धूल चटाई, जिसके पास कुछ बरसों पहले संसद में मुश्किल से दो सीटें थीं। फिर भी सत्ता का हस्तांतरण आसानी व सुगमता से हो गया। यहां कोई व्यापक उथल-पुथल नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध (कभी-कभी) और बढ़ती कीमतें छोड़ दें तो कोई राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी नहीं होते। मार्क्सवादियों ने जिस क्रांति के होने का अनुमान लगाया था, उसके कोई चिह्न नहीं हैं। तथ्य तो यह है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्हें हम माओवादी कहते हैं, उनका प्रभुत्व होने के बाद भी मार्क्सवादी गायब ही हो गए हैं। क्या हम इतने आलसी हैं कि विरोध ही नहीं करते? या हम जरा ज्यादा ही सौम्य हैं? या राजनीति के प्रति हमारे प्रेम के बाद भी हम अराजनीतिक लोग हैं? मुझे लगता है, इसमें से कोई बात लागू नहीं होती। हां, हममें से कई आलसी तो हैं। इतने आलसी कि उसके लिए भी उठकर लड़ने को तैयार नहीं, जो हमारा अधिकार है, इसीलिए इतना कुछ होने के बाद भी सरकार बच निकलती है। किंतु हम बड़े ही भले लोग हैं। और हां, हमें राजनीति पसंद तो है पर हम इसे बदलाव का जरिया मानने की बजाय मनोरंजन अधिक मानते हैं। समस्या यहीं पर है। यही वजह है कि हमारे यहां कभी थ्येनआनमन चौक या अरब वसंत जैसी घटनाएं होने की संभावना नहीं है। हमारे युवा नौकरियां खोजने और कॅरिअर बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वे उस आदर्शवाद को दोहरा नहीं सकते, जिसने 1960 के दशक में नक्सलबाड़ी आंदोलन और पेरिस विद्रोह को जन्म दिया था। उनके टी शर्ट पर चेग्वेरा का चेहरा बना हो सकता है पर उन्हें कुछ पता नहीं है कि चे किस बात के प्रतीक हैं। इसकी बजाय हमें तत्काल भड़ास निकालने के तीन माध्यम मिल गए हैं। खबरों के चैनल, ट्विटर और बॉलीवुड। ये हमें आज़ाद, मुक्त और आत्म-संतुष्ट महसूस कराते हैं। हमारे सारे गुस्से, सारी कुंठा को उसी से राह मिलती है। नक्सलबाड़ी आंदोलन कब लड़खड़ाने लगा था? सत्तर के दशक के मध्य में जब सिनेमा के परदे पर एंग्री यंगमैन अवतरित हुआ। हमारे लिए वह खलनायकों की पिटाई करता था। वह सूदखोरों को ठिकाने लगाता था। राजनेताओं और सत्ता के दलालों से नफरत करता। भ्रष्ट पुलिस वालों को घुटनों के बल ले आता। अमिताभ बच्चन लाखों युवाओं की कल्पनाओं को साकार करते तो वे खूब तालियां पीटते। वे अपनी भारी आवाज में उनके गुस्से को राह देते। बुद्धजीवी हमारे सिनेमा को पलायनवादी कहते हैं, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य पूरा करता है। उसने हमें राष्ट्र के रूप में एक साथ जोड़ रखा है। हमें हताशाओं से उबरने में मदद की है। जब नेहरू आधुनिक भारत के मंदिरों के निर्माण में लगे थे, हमारा युवा एकल परदे वाले सिनेमाघरों के अंधेरे में अपने वास्तविक सपनों को जी रहा था, भ्रष्टों, दुष्ट व्यवस्था की ठुकाई कर रहा था। फिर टेलीविजन आया और इसके साथ आए खबरिया चैनल। रूखा-सूखा, उबाऊ। यह हमें वही बताता, जो हम पहले से ही जानते थे और इस तरह इसने हमारी जिंदगी और असहनीय बना दी। फिर करीब आठ साल पहले एक और एंग्री यंगमैन आया और उसने खेल के सारे नियम बदल दिए। समाचार तत्काल रंगमंच में बदल गए। बुरे लोगों की पिटाई होने लगी। भ्रष्टों का भंडाफोड़ होने लगा, उन पर गुस्सा उतारा जाने लगा। विनम्रता की जगह खिंचाई ने ले ली। अर्नब गोस्वामी समाचार वाचक नहीं हैं। वे जज, जूरी और जल्लाद तीनों हैं। ऐसा नहीं कि राजनीतिक रूप से वे हमेशा ही सही होते हैं, लेकिन वे सही मुदनोदे के साथ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि सड़क के आदमी को क्या चाहिए। अमिताभ के खलनायकों की तरह उनके खलनायक भी अच्छे-बुरे का मिश्रण नहीं हैं। वे काले, पूरी तरह काले हैं। उनके नायक थोड़े ही हैं। मध्यवर्गीय भारत के लिए वे नायक हैं। एंग्री यंगमैन का नया रूप। उन्होंने नई शैली को जन्म दिया है। गुस्सैल, उन्मादी, भावनाओं को राह देने वाली और हां, मुक्त करने वाली। दूसरी तरफ ट्विटर को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती। यह भड़ास निकालने की आपकी व्यक्तिगत मशीन है। आप वहां जाकर चीख सकते हैं, कोस सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। सलमान खान के फैमस शब्दों में कहें तो ‘डू व्हाटेवर यू वांट, मैन।’ यदि इससे आप थोड़े मूर्ख नजर आते हैं तो चिंता न करें। कोई ध्यान नहीं देगा। यदि ध्यान दें भी तो अपना ट्विटर हैंडल बदल लीजिए। आपकी गुमनामी आपकी ताकत बन जाएगी। आप पत्नी से नफरत करते हैं, जाइए और सारी पत्नियों को कोसिए। पड़ोसी से घृणा है, जाइए और सारे पड़ोसियों को निशाना बनाइए। आपके पीछे गली का कुत्ता पड़ गया? मांग कीजिए कि सारे आवारा कुत्तों को मार डाला जाए। अपनी नफरत व गुस्से की दुनिया निर्मित कीजिए। गुस्सा जताएं, शिकायतें करें और विघ्नसंतोषी बन जाएं। और अपने जैसे लोगों का समूह बनाकर नए हीरो, नए विलैन तैयार करें। जब तक बॉलीवुड फल-फूल रहा है और न्यूज टीवी व ट्विटर हैं, भारत में किसी तरह के बगावती तेवर देखने को नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि वे कहने को चाहे जो कहें पर हर सत्ता इन तीनों से प्रेम करती है। वे भारत को क्रांतिकारियों के हाथों से दूर जो रखते हैं। प्रीतीश नंदी फिल्म निर्माता और वरिष्ठ पत्रकार pritishnandy@gmail.com