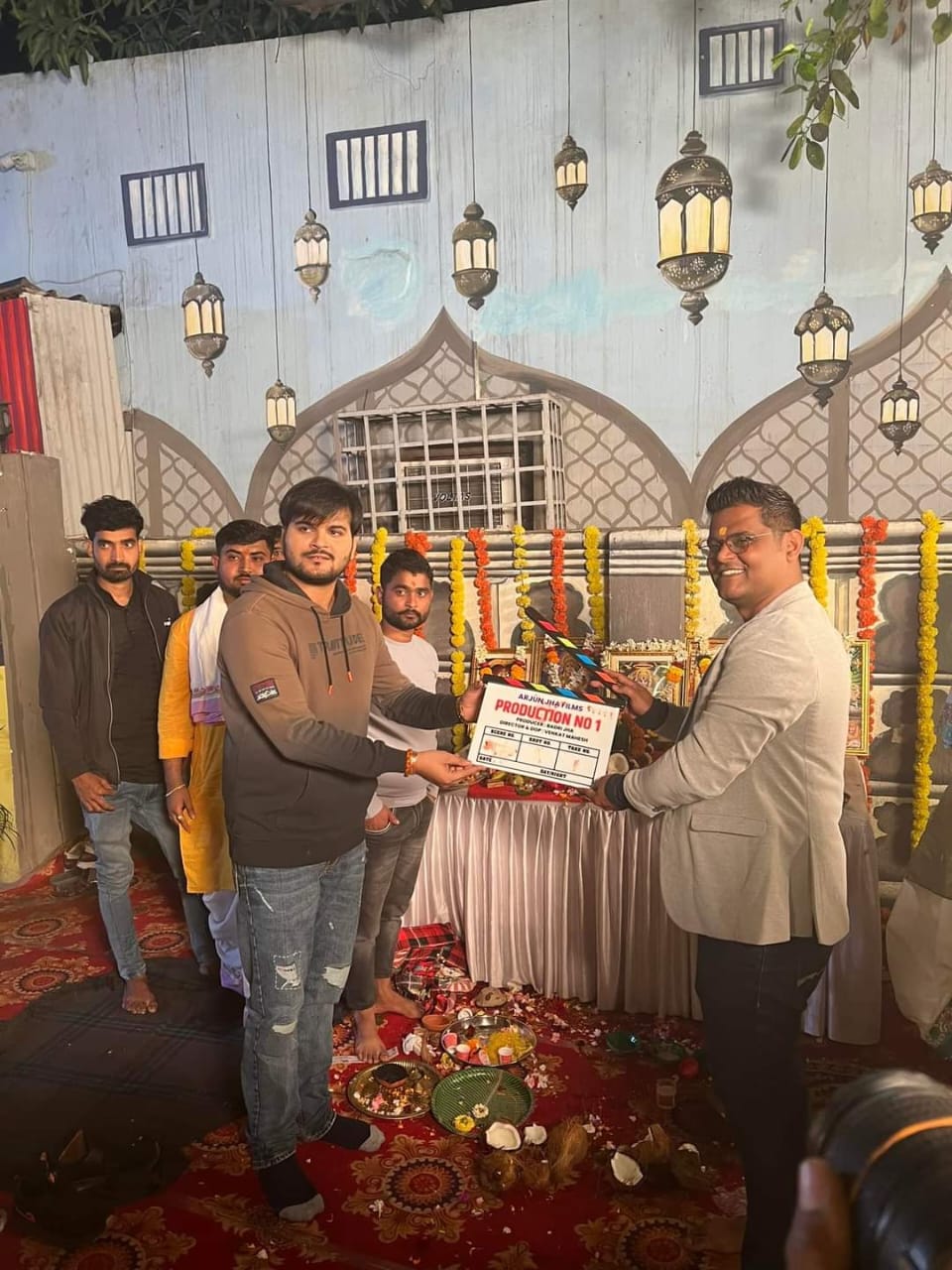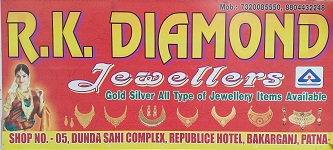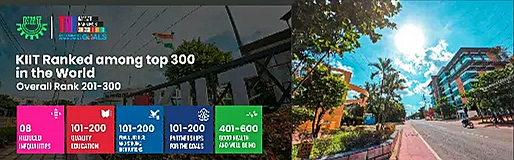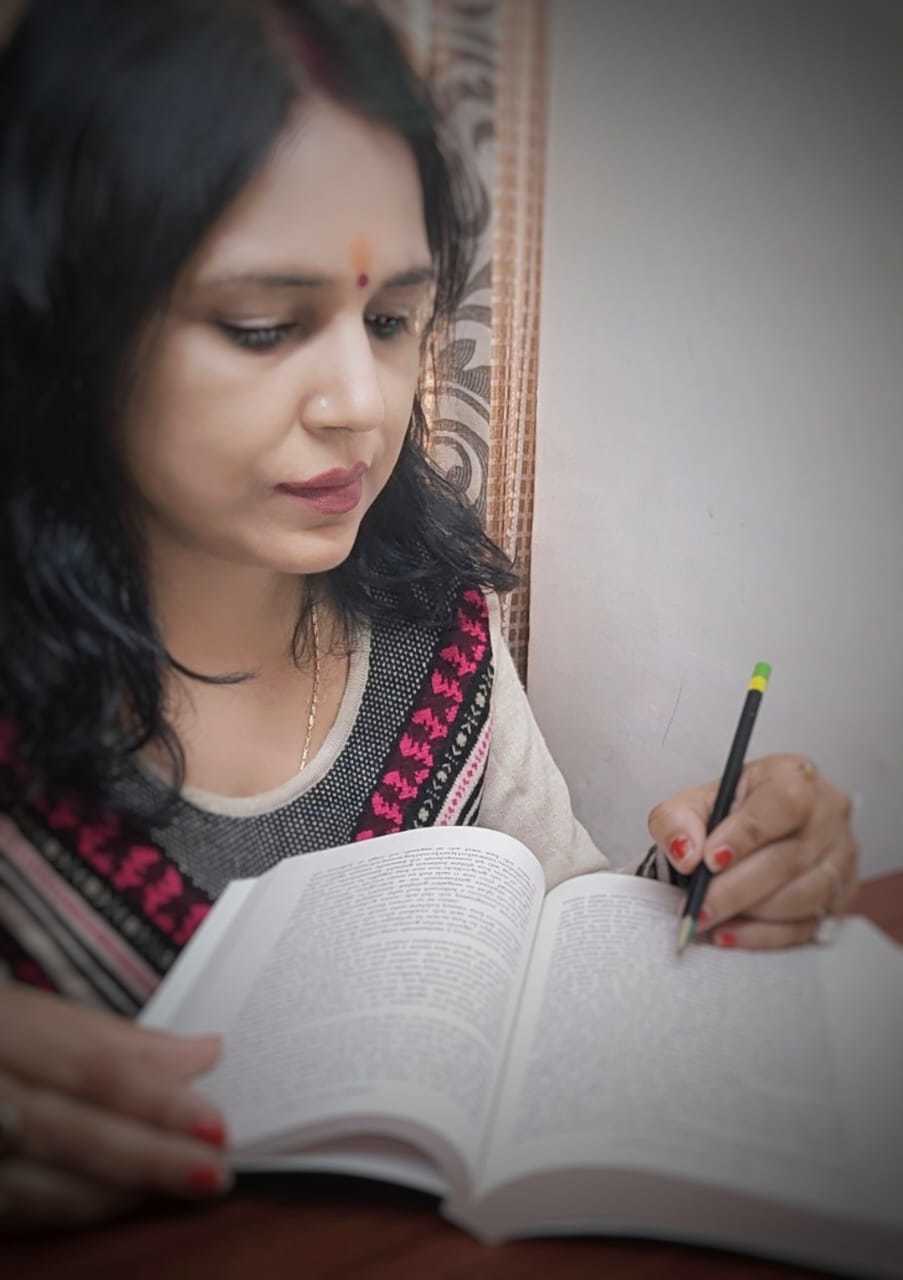सरदार पटेल : भारत के अविस्मरणीय लौहपुरुष
आज पुण्यतिथि है उस महान नायक की जो एक पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानी थे और दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता भी. उस प्रतापी राजपुरु ष का स्मरण आते ही मन भय और श्रद्धा के मिश्रित भाव से भर जाता है. सरदार वल्लभभाई पटेल जिन्हें भारत का लौह-पुरुष माना जाता है. उनकी प्रबल लालसा थी कि मरने के बाद लोग उनके बारे में कहें- ‘‘वह बोलता था तो कुछ कड़ी बातें भी कहता था, मगर आदमी ठीक था.’’ लाजिमी है कि उनकी कही वैसी कुछ तीखी बातों का जिक्र प्रसंगानुकूल हम करते चलें. यह इसलिए भी जरूरी होगा, ताकि नयी पीढ़ी को ठीक मालूम हो जाये कि सरदार कौन थे और उन्होंने हमारे हित में क्या कहा और क्या किया. उन दिनों भारत के प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मगर जब तक सरदार वल्लभभाई पटेल जीवित रहे, घर के असल मालिक-मुख्तार वे ही माने गये. एक तरह से पार्टी और सरकार, दोनों के गार्डियन. हालांकि गांधीजी की मृत्यु के बाद वे पंडितजी को ही अपना नेता बताते और कहते, ‘‘यदि मैं अपने लीडर का साथ न दे सकूं और उनके हाथ मजबूत न कर पाऊं तो एक मिनट भी गवर्नमेंट में नहीं रहूंगा.’’ लेकिन उनकी हकीकी हैसियत का इजहार करते हुए खुद पंडितजी ने प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एडगर स्नो को बताया था : ‘‘मैं जानता हूं कि इशारा कर दूं तो सरदार मंत्रिमंडल छोड़ देंगे और वे भी जानते हैं कि उनका इशारा पाते ही मैं सरकार से बाहर निकल आऊंगा.’’ कांग्रेस में उनकी धाक की एक वजह यह भी थी कि पार्टी आला कमान में गांधीजी को छोड़ बाकी सबसे वे उम्र में बडे थे. राजाजी, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, नेहरू, सुभाष बोस- सब उनसे छोटे थे. पंडितजी तो चौदह साल छोटे थे और सुभाष बीस साल. सरदार पटेल एक कुशल संगठनकर्ता थे और पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ का एक कारण यह भी था कि सन 1936-37 के जमाने से ही कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के वे अध्यक्ष रहते आये थे और उस नाते पार्टी उम्मीदवारों के चयन और प्रादेशिक मंत्रिमंडलों के गठन जैसे अहम मामलों में उनका वर्चस्व सदा बना रहा. और तो और, केंद्रीय पार्टी कोष के प्रमुख संग्रहकर्ता भी वे ही रहे. जनसाधारण और धनवानों का उन पर इतना विश्वास था कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के लिए हफ्ते-दो हफ्ते में ही दस लाख रु पये झोली में भर लाये. उस जमाने (1920) में दस लाख बहुत बड़ी रकम होती थी. और यह भी ध्यान रहे कि तब वे कोई सत्ताधारी भी नहीं थे. स्वतंत्रता इतिहास को संभल कर पढ़ें तो लगेगा गांधी, नेहरू और पटेल मानो एक-दूसरे के पूरक रहे हों. ऐसा नहीं कि अलग-अलग मुद्दों पर उनमें आपसी मत-भिन्नता न थी. लेकिन मुल्क की नब्ज गांधी सबसे ज्यादा ठीक पहचानते थे. नतीजे हर बार बताते कि गांधी का कहना सही था. और उनके नैतिक बल का तो कहना ही क्या! इसलिए, मन-मिजाज और रु झान की भिन्नता के बावजूद जिन तीन बातों ने नेहरू और पटेल को आपस में बांध रखा था, वो थीं देश की आजादी, पार्टी की साख और बापू के प्रति निष्ठा. कहना अनावश्यक है कि त्याग, संघर्ष और कष्ट-भोग में पटेल और नेहरू एक जैसे थे. गांधी के प्रिय और अंतरंग दोनों ही थे. वल्लभभाई अनुजतुल्य तो जवाहरलाल पुत्रवत. बापू दोनों के मोल-महत्त्व को अच्छी तरह जानते थे. पटेल के तथ्यपरायण विवेक के गांधी इतने कायल थे कि बारदोली सत्याग्रह के दिनों में लार्ड इरविन को लिखा था कि जो समाधान सरदार को स्वीकार्य न हो वह उन्हें भी कदापि मान्य न होगा. तथापि, प्रधानमंत्री पद के लिए वे नेहरू की ओर अधिक उन्मुख बताये गये हैं तो मेरा कयास है कि प्रांतवाद की अनावश्यक लांछना से शायद वे हिचक गये होंगे; क्योंकि गांधी और पटेल दोनों ही गुजराती थे. लोगों का क्या, कुछ भी अनर्गल बक सकते हैं! मुमिकन है गांधी के मन में इसकी आशंका रही हो. बहरहाल, हमारा सौभाग्य था कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाये गये और उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल. पंडितजी का सर सदा आकाश की ऊंचाइयों की ओर उठा होता, सरदार के पांव बराबर धरती पर मजबूती से जमे रहते थे. वल्लभभाई में सच्चाई और साहस कूट-कूट कर भरा था. जो बात ईमानदारी से महसूस करते, उसे दो-टूक कहने की हिम्मत रखते थे. लोकमंगल और जनसेवा के भाव से सत्ता संभाली थी और कर्त्तव्यबोध से ही सदा प्रेरित होते रहे. एक तरफ उनके त्याग और सदाचार का लोग सम्मान करते, तो दूसरी ओर उनकी सख्ती से भी सब घबराते थे. अकड़ तो किसी की भी उन्हें बर्दाश्त थी ही नहीं. एक घटना हमारे बिहार की है, जहां आकाशवाणी के पटना केंद्र का उद्घाटन करने वे आये थे. उस शाम हुई जनसभा में जमींदारी मुआवजे के प्रश्न पर बिहार सरकार को उन्होंने खरी-खोटी सुना दी. मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉ श्रीकृष्ण सिंह थे. अपनी सरकार की सार्वजनिक निंदा से बौखला कर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली. खबर लेकर सत्यनारायण बाबू (भारत सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जो बिहार के ही थे) जब सरदार के पास पहुंचे तो उन्होंने इतना ही कहा, ‘‘ठीक है, जाकर श्रीबाबू से कह दो कि गवर्नर को फौरन इस्तीफा दे आयें. मैं कल नयी सरकार बनवा कर ही दिल्ली लौटूंगा.’’ इतने से ही सब की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी. लेकिन आप यह न मान बैठें कि सरदार केवल धौंस के ही धनी थे. उनमें राजनीतिक सूझ-बूझ और कूटनीतिक कौशल भी भरपूर था. व्यूह रचना के तो वे माहिर थे. इशारे में बस इतना ही कह दूं कि सरदार अगर राजी न होते तो कतई मुमिकन न था कि सत्ता हस्तांतरण के बाद भी एक साल तक लार्ड माउंटबेटन आजाद भारत के गवर्नर जनरल बने रह जाते. जिन्ना साहब तो उस योजना को सिरे से खारिज कर पाकिस्तान के उस आला ओहदे पर खुद काबिज हो गये. अपने प्रति नेहरू और पटेल की उस सम्मिलित सौजन्यता का माउंटबेटन ने भी मुनासिब सिला दिया. उस दौर के इतिहास को खंगालेंगे तो देसी रियासतों को भारत के पक्ष में लामबंद करने में माउंटबेटन की गुप्त भूमिका छन कर निकल आयेगी. लेकिन 563 रजवाड़ों के भारत में विलय का सर्वाधिक श्रेय नि:संदेह सरदार पटेल को ही जायेगा. उन्हें वह हुनर बखूबी मालूम था कि लोहे को कितना गर्म किया जाये और उस पर कब चोट मारी जाए. इसलिए, राजे-महाराजों को पहले तो उन्होंने अनुरागपूर्वक समझाया कि जब भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, तो क्यों न राजनैतिक तौर पर भी एक हो जाएं? लेकिन जब महाराजे-नवाबों में खुदसरी के हौसले हिलोरे लेने लगे तो सरदार की भाषा बदली और उन्होंने आगाह किया कि भारत की आजादी के बाद देसी रियासतों में भी निर्वाचित उत्तरदायी सरकार की मांग जोर पकड़ेगी जो राजघरानों को हरगिज गवारा न होगा. उस स्थिति में जन-आंदोलन को कुचलने के लिए यदि बल प्रयोग किया गया, तो निश्चय ही भारत सरकार की पूरी सहानुभूति प्रजाजनों के साथ होगी. राजे-महाराजे सरदार का राजसी संकेत समझ गये. 15 अगस्त 1947 की अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले ही कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ बाकी सभी राजवाड़े भारतीय संघ के अभिन्न अंग बन चुके थे. जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान के बहकावे में आ गये. भारत के आंतरिक सुरक्षा बल ने जूनागढ़ को धर दबोचा. पाकिस्तान जब शोर मचाने लगा तो गृहमंत्री पटेल ने ललकारा, ‘‘आप क्यूं जूनागढ़ के दरवाजे पर आ बैठे? वहां तक कहां से आया पाकिस्तान? आपके कहने से ही हिंदुस्तान के दो टुकड़े किये गये. उसके बाद और टुकड़े करने हों तो मैदान में खुली बातें करो.’’ पाकिस्तान के वजीरे-खारिजा (विदेश मंत्री) जफरुल्ला खान यूएनओ जाने को बेताब हो उठे. सरदार ने एक सार्वजनिक सभा में कहा- ‘‘जूनागढ़ का फैसला तो अब हो गया. यूएनओ जाओ चाहे जहां जाओ. कोई नयी बात नहीं बन सकती.’’ कश्मीर के मामले को सरदार यूएनओ भेजने के पक्ष में न थे. माउंटबेटन की कच्ची सलाह और पंडितजी के हठ से मामला नाहक पंचैती में फंस गया. लेकिन तकरार जब सुपुर्दे-अदालत हो ही गया तो जनाब जफरु ल्ला खुद हाय-तौबा मचाने लगे. सरदार ने सार्वजनिक मंच से कहा- ‘‘जफरुल्ला साहब कहते हैं कि आप वहां (यूएनओ) क्यूं गये?.. ठीक है, यदि वह चाहते हैं तो हम अपनी अर्जी वापस ले लेंगे. मगर हमें बताइये कि तब (कश्मीर जाने का) दूसरा रास्ता क्या होगा? फिर तो हमें स्यालकोट और लाहौर होकर जाना पड़ेगा.’’ जफरु ल्ला को आफत अपनी ओर बढ़ती नजर आयी. अरसे तक वे खामोश बैठे रहे. कुछ बकवासी लोगों का ख्याल है कि आजादी के कबल बनी चंदरोजा अंतरिम सरकार में मुसलिम लीग के प्रतिनिधि मंत्रियों का गृहमंत्री पटेल लगातार मानमर्दन न कर रहे होते तो मुमिकन था जिन्ना साहब भारतीय संघ में बने रहने पर राजी हो जाते. दरअसल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शरीक ही इस इरादे से हुई थी कि पाकिस्तान की अपनी लड़ाई वह ज्यादा मजबूती से लड़ सके. लीग के नुमाइंदे जिस दिन (अक्तूबर 1946) से मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसी दिन से सरकार सांप्रदायिक राजनीति का समरक्षेत्र बन गयी. लीगी वजीर न तो नेहरू को सरकार का प्रधान मानते थे और न खुद को उनके प्रति उत्तरदायी. वे लोग लियाकत अली खान की सदारत में अपनी अलग से कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक करते रहे. साझा कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रस्तावों के विरोध में अमूमन अपने वीटो पॉवर का प्रयोग कर बैठते. उन लोगो ने प्रशासनिक माहौल इतना बिगाड़ दिया कि ऊपर सचिव स्तर के अधिकारी से नीचे चपरासी तक मन ही मन सांप्रदायिक आधार पर इस तरह बंट गये मानो दो सामानांतर सरकारें चल रही हों. आजिजी में न केवल पटेल, बल्कि नेहरू ने भी मुल्क का बंटवारा बेहतर समझा. सरदार पर ज्यादातर प्रहार वामपंथी खेमे से हुआ करते थे जिसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों पार्टियां शामिल थीं. उनकी नजरों में पटेल प्रतिगामी, पूंजीपतियों के पोषक और सांप्रदायिक थे. यह तो ठीक है कि उद्योगपति और धनवानों से सरदार के अच्छे सरोकार रहे. समय-समय पर सार्वजानिक कार्य के लिए उनसे काफी पैसे भी मिल जाया करते थे. लेकिन सार्वजनिक कोष का एक पैसा भी वल्लभभाई ने कभी निजी प्रयोजन में खर्च नहीं किया और न तो उनलोगों से कोई व्यक्तिगत लाभ उठाया. इसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि उनकी इकलौती बेटी मणिबेन, जो आजीवन अविवाहिता रह गयीं और अंत तक पिता की सेवा में जुटी रहीं, सरदार की मृत्यु के बाद अहमदाबाद के सिंगल बेडरूम वाले फ्लैट में बसर करने लग गयी थीं. सरदार यदि वामपंथियों की नीति और कार्यक्र मों के खिलाफ थे, तो उसके वैचारिक कारण थे. वे कहते : ‘‘अगर मुङो समझ आ जाए कि हमारे मुल्क में एक-एक कैपिटलिस्ट की कैपिटल खत्म कर देने से हिंदुस्तान का भला होगा, तो उसे खत्म करने में मेरा नंबर पहला रहेगा. ..आप कहते हैं कि मजदूरों को पैसा मिले, उनकी जरूरतें पूरी हों. तो इस काम में आपको मेरा पूरा साथ मिलेगा. (मगर) हिंदुस्तान को तो अभी आजादी मिली है. हम दो-चार साल कुछ इंडस्ट्री लगा लें, कुछ उद्योग पैदा करें. तभी तो मजदूरों के लिए भी कुछ धन पैदा हो सकेगा और उन्हें हिस्सा मिलेगा. जहां होगा, वहीं से तो कुछ दिया जा सकेगा. तो पहले कुछ पैदा करो.. मुङो सोशलिज्म सिखाने की किसी को जरूरत नहीं. जब से मैंने गांधीजी का साथ पकड़ा तभी से फैसला किया कि पब्लिक लाइफ में काम करना हो तो अपनी मिलकियत नहीं रखनी चाहिए. तब से आज तक न मेरा कोई बैंक अकाउंट है, न मेरे पास कोई जमीन है और न अपना कोई मकान.. उससे भी आगे जाना पड़े तो मुकाबला करने को तैयार हूं. लेकिन हिंदुस्तान की बर्बादी में कभी साथ नहीं दूंगा. उससे आप कहें कि मैं कैपिटलिस्टों का एजेंट हूं या जो चाहे सो नाम दो..’ सरदार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाना बौद्धिक बेईमानी होगी. यह ठीक है कि पाकिस्तान, भारतीय मुसलमान और दिल्ली दंगे के प्रति गृहमंत्री के रु ख के कारण नेहरू-पटेल मतभेद इतना तीखा हो गया था कि सरदार ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. उन दिनों स्वयं गांधीजी उन्हीं प्रश्नों को लेकर उपवास कर चुके थे, जिसका परोक्ष अर्थ हो जाता था गांधी द्वारा पटेल की मौन निंदा. इसलिए, सरदार ने भी अपना त्यागपत्र गांधीजी के पास ही भेजा था. उस दौर में सबसे ज्यादा खलबली लखनऊ में दिये गये सरदार के उस भाषण से मची थी जिसमे उन्होंने कहा था : ‘‘आपका यह